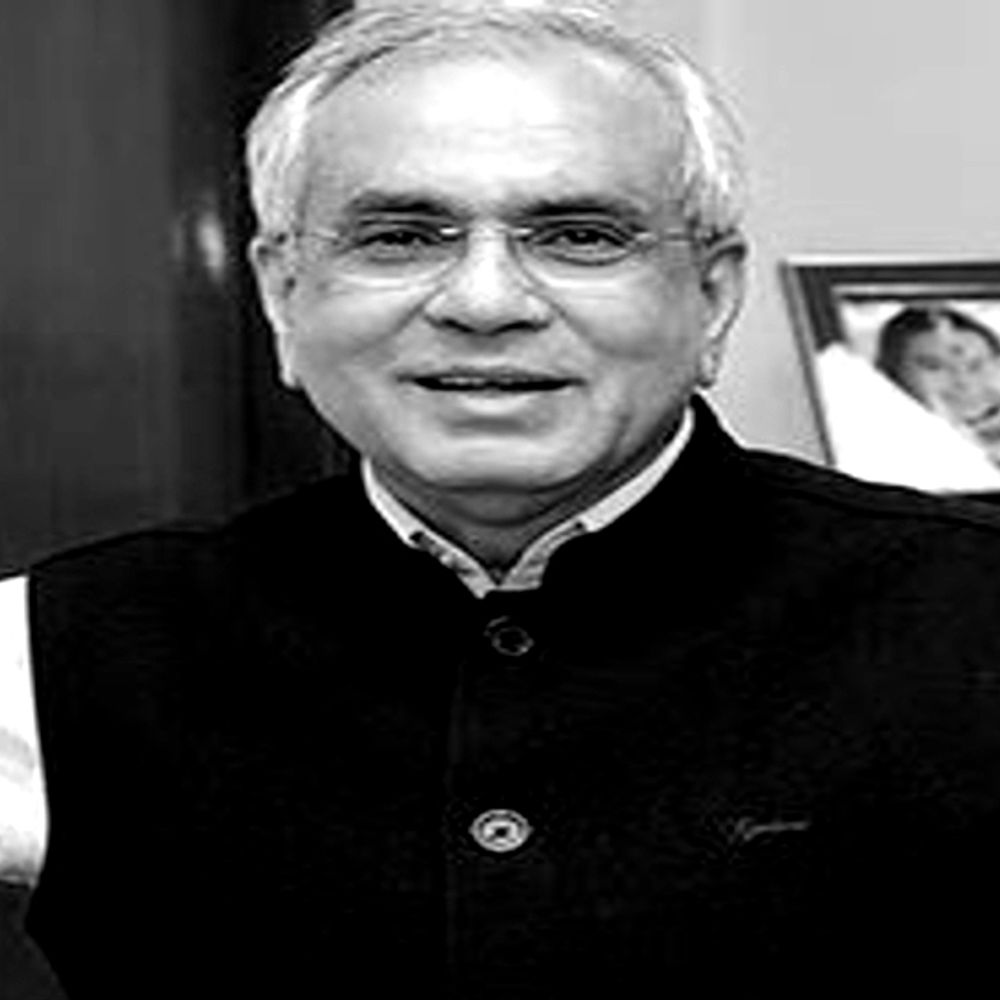
डॉ. राजीव कुमार का कॉलम:हमें अपने खेती करने के तरीकों में अब बदलाव लाना होगा
Published at : 2025-06-26 00:30:00
सघन कृषि के समर्थकों का मत है कि भारत की मौजूदा कृषि प्रणाली समय के साथ उत्पादन में बढ़ोतरी कर देश की खाद्य सुरक्षा में सहायक बनी रहेगी। हालांकि, कृषि संबंधी डेटा इस विचार का समर्थन नहीं करते हैं। कई साक्ष्य बताते हैं कि देश में मिट्टी के उपजाऊपन, भूजल संसाधन और उर्वरकों की क्षमता बिगड़ती जा रही है। रुझान बताते हैं कि अगले दशक में गेहूं, चावल जैसे खाद्यान्न का उत्पादन गिरेगा। वहीं खाद्यान्न की मांग हर साल 2 से 3 प्रतिशत बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिक तौर पर इस बात का कोई सबूत नहीं कि मौजूदा सघन कृषि प्रणाली देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगी। हमें सघन कृषि प्रणाली (ऐसी पद्धति, जिसमें कम भूमि से अधिक उपज प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है) के बजाय ऐसा तंत्र विकसित करना होगा, जो ज्यादा स्थायी और भरोसेमंद हो। यह साबित हो चुका है कि प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग वाली वैकल्पिक कृषि प्रणालियों से कैसे किसानों की आय और उत्पादन को दोगुना किया जा सकता है। ऐसी प्रणालियों को आम तौर पर प्राकृतिक या री-जनरेटिव खेती कहा जाता है। भारत में कुल किसानों का महज 5 प्रतिशत यानी सिर्फ 20 से 30 किसान ही ऐसी खेती करते हैं। लेकिन ये सब लघु और सीमांत किसान हैं, जो बाजार नहीं, जीवनयापन के लिए फसल उगाते हैं। बाजार के लिए उत्पादन करने वाले किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति आकर्षित करने के लिए हमें तथ्य जुटाने होंगे। प्राकृतिक कृषि प्रणाली से किसान व उपभोक्ता की बेहतर सेहत, पर्यावरण स्थायित्व और सामाजिक समावेश जैसे लाभ हैं। आज आवश्यकता है कि हम इसकी व्यावहारिकता और गुणों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा शुरू करें। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर बनाया गया जनमानस भारतीय कृषि में बदलाव के लिए उत्पादक, उपभोक्ता और समाज के बीच सहमति बनाने में सहायक होगा। इसके लिए देश में दोनों प्रकार की कृषि प्रणालियों को लेकर अध्ययन कराया जाना चाहिए, जो उत्पादकता, कृषक आय, मृदा स्वास्थ्य, जैव विविधता, पोषकता समेत विभिन्न सामाजिक व स्वास्थ्य सूचकांकों को लेकर मजबूत वैज्ञानिक साक्ष्य दे पाए। प्राकृतिक खेती के जरिए आज किसानों को बिजली, पानी और उर्वरकों के लिए दी जा रही वित्तीय रियायतों का वजन भी कम होगा। इस बचत से सघन से प्राकृतिक की ओर बढ़ रही कृषि प्रणाली को सहायता देने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाए जा सकते हैं। किसी भी कृषि प्रणाली को उत्पादकता, आय, पोषकता और विविधता के संदर्भ में जरूर देखा जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश में समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती (सीएनएफ) की ऐसी ही प्रणाली का मूल्यांकन किया जा रहा है। एक ताजा रिपोर्ट में बताया गया कि इस प्रणाली के जरिए चावल, मक्का, मूंगफली, रागी जैसी प्रमुख उपजों में 7.8 से 25.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इससे किसान की लागत कम हुई और उनकी सकल आय में भी 28.3 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई। हालांकि, ये साक्ष्य उत्साहजनक हैं, लेकिन सीमित भूभाग के लिए हैं। अन्य लाभों के अलावा प्राकृतिक खेती में कार्बन अवशोषण और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने की क्षमता भी औद्योगिक खेती की तुलना में अधिक है। अगर इस खेती के सभी लाभों को देखें तो यह देश में कार्बन उत्सर्जन रहित "नेट जीरो एग्रीकल्चर' के साथ भारतीय किसान के लिए बेहतरीन स्थिति हो सकती है। प्राकृतिक खेती को लेकर देश में बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक अध्ययन के जरिए भरोसेमंद तथ्य जुटाए जाएं तो किसानों की चिंताओं को दूर किया जा सकता है। कृषि शिक्षा और शोध की शीर्ष निकाय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को भी इसमें भूमिका निभानी चाहिए। यदि प्राकृतिक और री-जनरेटिव खेती में निवेश किया जाए तो यह मौजूदा सघन कृषि प्रणाली का विकल्प हो सकती है। इस खेती को प्रोत्साहन देने से देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी और यह 2070 तक हमारे 'नेट जीरो' के संकल्प को भी पूरा करने में सहायक होगी। (ये लेखक के अपने विचार हैं। इसके सहलेखक फेडरेशन यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया के डॉ. हरपिंदर संधू हैं)
